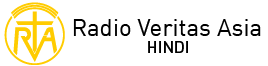भारत के जलवायु-प्रभावित संघर्ष क्षेत्र में खेतों को पुनर्जीवित करने का एक व्यक्ति का मिशन

स्वर्ण लाल, जो लगभग पचास वर्ष की आयु के एक दुबले-पतले व्यक्ति हैं, जिनके गाल धूप से झुलसे हुए हैं और जिनकी मुस्कान बेहद आकर्षक है, अपने खेत में बासमती चावल के लहराते पन्ने जैसे डंठलों के बीच खड़े हैं, जो क्षितिज से बिल्कुल अलग है, जहाँ अक्सर सेना की चौकियाँ और काँटेदार तार की बाड़ें दिखाई देती हैं।
लाल का गाँव, सुचेतागढ़, भारतीय कश्मीर के जम्मू जिले में, पाकिस्तान की सीमा के पास है। इसका मनोरम परिदृश्य संघर्ष के निशानों और जलवायु परिवर्तन के निरंतर प्रभाव, दोनों से चिह्नित है।
हालाँकि, इस अकेले किसान का दृढ़ संकल्प अनिश्चित भविष्य के साथ तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष कर रहे इस क्षेत्र के लिए आशा की किरण बन गया है।
अप्रशिक्षित आँखों को, उनके खेत इस क्षेत्र के किसी भी अन्य धान की तरह ही लगते हैं। लेकिन सतह के नीचे, लाल ने एक शांत क्रांति की शुरुआत की है: जैविक, जलवायु-प्रतिरोधी खेती।
“इस कठिन समय में, हर बीज एक प्रार्थना है। धरती हमारी माँ है। अगर हम उसके लिए नहीं बदलेंगे, तो कौन बदलेगा?” लाल ने यूसीए न्यूज़ को बताया।
भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनाव और बीच-बीच में होने वाली झड़पों ने सीमावर्ती गाँव में जीवन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।
लेकिन हाल के वर्षों में, जलवायु ही इसकी सबसे अप्रत्याशित दुश्मन बन गई है।
कभी भरोसेमंद मानसून अनियमित हो गया है, गर्मी की लहरें लंबे समय तक चलती हैं, और बेमौसम बारिश ने फसलों को खतरे में डाल दिया है।
लाल जैसे किसानों के लिए, जिनकी आजीविका पूरी तरह से मौसम की अनिश्चितताओं पर निर्भर करती है, दांव इससे ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता।
लाल ने कहा, “पहले, हमें पता होता था कि बारिश कब आएगी। हम अपनी बुवाई और कटाई की योजना उसी के अनुसार बनाते थे। अब, आसमान हमें धोखा दे रहा है। कभी महीनों तक सूखा रहता है, तो कभी रातों-रात बाढ़ आ जाती है। यह डरावना है।”
जब 2010 के दशक के मध्य में एक के बाद एक फसलें बर्बाद हुईं, तो सुचेतागढ़ के कई लोगों ने अपने पुश्तैनी खेतों को छोड़ने के बारे में सोचा।
लेकिन लाल पहले से ही एक अलग रास्ता चुन चुके थे, इसलिए वे तैयार थे।
फसल उत्पादन में गिरावट
जलवायु परिवर्तन ने जम्मू और कश्मीर में कृषि और बागवानी को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे फसल उत्पादन और गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
यह क्षेत्र, जहाँ लगभग 80 प्रतिशत कार्यबल कृषि में कार्यरत है, बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, सूखे, ओलावृष्टि और बाढ़ के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है।
उदाहरण के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में कुल कृषि उत्पादन 2019 में 3,936.230 टन से घटकर 2020 में 3,912.910 टन रह गया।
सेब, अखरोट और केसर जैसी बागवानी फसलें - जो कई लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं - बढ़ते तापमान, कम वर्षा और सस्ती फसलों के आयात के कारण प्रभावित हुई हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले दो दशकों में कश्मीरी केसर का उत्पादन 65 प्रतिशत घटकर 16 मीट्रिक टन से मात्र 5.6 मीट्रिक टन रह गया है।
अखरोट का उत्पादन, जिसमें जम्मू और कश्मीर भारत के कुल उत्पादन का 92 प्रतिशत हिस्सा रखता है, भी प्रभावित हुआ है।
इन बदलावों ने पारंपरिक कृषक समुदायों पर दबाव डाला है, जिससे कई लोग वैकल्पिक फसलों या आजीविका पर विचार करने को मजबूर हुए हैं, जिससे इस क्षेत्र में जलवायु-प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों और नीतिगत हस्तक्षेपों की तत्काल आवश्यकता उजागर हुई है।
लाल का दृढ़ संकल्प
जलवायु परिवर्तन का सीधा सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित, लाल ने जैविक तरीकों के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया था।
उन्होंने अपनी फसलों में विविधता लाई, मिट्टी की उर्वरता बहाल करने के लिए चावल के साथ दालें और सब्ज़ियाँ उगाईं।
रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की जगह घर में बनी कम्पोस्ट और नीम (महोगनी परिवार का एक पेड़) आधारित जैविक कीटनाशकों ने ले ली। टपक सिंचाई ने बेकार बाढ़ की जगह ले ली, जिससे बहुमूल्य भूजल का संरक्षण हुआ।
शुरू में, उनके पड़ोसी संशय में थे।
"लोग मुझे पागल कहते थे। वे कहते थे कि जैविक खेती उन लोगों के लिए है जो असफल होने का जोखिम उठा सकते हैं," लाल हँसते हुए कहते हैं। "लेकिन मेरा मानना था कि अगर हम नहीं बदले, तो हम सब कुछ खो देंगे।"
उनका यह विश्वास जल्द ही फलित हुआ।
लाल के सुगंधित और रासायनिक अवशेषों से मुक्त जैविक बासमती चावल को स्थानीय बाज़ारों में अच्छी कीमत मिली।
जब 2018 में एक खेप अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में पहुँची, तो यह न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे गाँव के लिए गर्व का क्षण था।
2020 में, जैसे-जैसे जलवायु संबंधी चुनौतियाँ बढ़ती गईं, कैथोलिक सोशल सर्विस सोसाइटी (सीएसएसएस) ने लाल के प्रयासों पर ध्यान दिया।
परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में उनकी क्षमता को पहचानते हुए, सीएसएसएस ने आरएस पोरा उपजिले में जलवायु-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया।