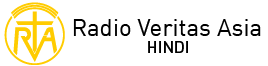पुरोहित मौन निराशा में मर रहे हैं

भारत में कैथोलिक कलीसिया एक ऐसे संकट का सामना कर रहा है जिसे वह शायद ही स्वीकार करता है। अपने परिचित रीति-रिवाजों और पल्ली कर्तव्यों के पीछे, पुरोहित खतरनाक दर से अपनी जान ले रहे हैं। ये कोई छिटपुट त्रासदियाँ नहीं हैं - ये उस व्यवस्था के बारे में चेतावनी हैं जो पूर्णता की माँग करती है, लेकिन बहुत कम समर्थन देती है।
हर 4 अगस्त को, चर्च पल्ली पुरोहितों के संरक्षक संत, संत जॉन वियान्ने का पर्व मनाता है। क्यूरे डी'आर्स के नाम से प्रसिद्ध, 19वीं सदी के इस फ्रांसीसी पुरोहित ने अपनी पवित्रता और अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्धि पाई। उन्होंने अनगिनत घंटे धर्मोपदेश में बिताए, कम सोते थे, कम खाते थे, और खुद को अपने बुलावे के अयोग्य मानते थे। उनका चित्र पूरे भारत में पवित्र स्थानों पर लगा है, जो पुरोहित जीवन के लिए एक आदर्श उदाहरण है।
लेकिन इस श्रद्धा का एक खतरनाक साया भी है। वियान्ने का चरम तप और मनोवैज्ञानिक संघर्ष एक आध्यात्मिक खाका बन गया है जिसका अनुसरण करने के लिए बहुत से भारतीय पादरी दबाव महसूस करते हैं। संदेश स्पष्ट है: सच्ची पवित्रता का अर्थ है मौन पीड़ा, अंतहीन त्याग और व्यक्तिगत आवश्यकताओं का परित्याग।
इसके परिणाम हृदयविदारक हैं। पिछले पाँच वर्षों में ही, मीडिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कम से कम 13 कैथोलिक पादरियों ने आत्महत्या कर ली है। औसतन, हर छह महीने में एक पादरी आत्महत्या करता है। इस वर्ष के पहले पाँच महीनों में ही दो पादरियों ने आत्महत्या कर ली है। क्या यह त्रासदी और भी विकराल होती जा रही है?
अधिकांश पीड़ित 30 से 50 वर्ष की आयु के हैं और अपने धर्मप्रांत में गंभीर मानसिक कष्ट और संघर्षों का वर्णन करते हुए नोट छोड़ते हैं। ये कमज़ोर आस्था वाले व्यक्ति नहीं थे। वे एक ऐसी व्यवस्था के शिकार हैं जो पीड़ा से निपटने के बजाय उसे आध्यात्मिक बना देती है।
आज के भारतीय पादरियों को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनकी वियान्ने ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे कम संसाधन वाले पल्ली में, अक्सर अकेले, जातिगत तनाव और घोर गरीबी से बँटे समुदायों की सेवा करते हैं। पिछली पीढ़ियों के विपरीत, अब उन्हें स्वतः ही सम्मान नहीं मिलता। इसके बजाय, उन्हें निरंतर जाँच, घटते व्यवसायों और चर्च के प्रति बढ़ती उदासीनता का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा, डिजिटल निगरानी उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखती है और सोशल मीडिया आलोचना को बढ़ावा देता है। पादरी वर्ग के अधिकार की पुरानी निश्चितताएँ अब बिखर गई हैं।
फिर भी, अपेक्षाएँ वही रहती हैं। पादरियों से अब भी यही अपेक्षा की जाती है कि वे सदाचार के आदर्श बनें, हमेशा उपलब्ध रहें और भावनात्मक रूप से स्थिर रहें। जब उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें और अधिक प्रार्थना करने, अधिक समय तक उपवास रखने और और भी अधिक विश्वास करने के लिए कहा जाता है।
यह विचार कि उन्हें पेशेवर मदद, सच्ची दोस्ती, या बस अपनी मानवता की स्वीकृति की आवश्यकता हो सकती है, अक्सर एक आध्यात्मिक कमज़ोरी के रूप में देखा जाता है।
यह हानिकारक संस्कृति मदरसों में शुरू होती है, जहाँ मनोवैज्ञानिक जाँच सतही रहती है और मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा से बचा जाता है। भावी पादरी जल्दी ही सीख जाते हैं कि भावनात्मक संकट को स्वीकार करना असफलता के बराबर है, पवित्रता का अर्थ है धैर्य, और मदद माँगना कमज़ोरी को उजागर करता है।
जब पादरी आत्महत्या करते हैं, तो संस्थागत प्रतिक्रिया अपेक्षित रूप से अपर्याप्त होती है। धर्मप्रांत शांत प्रार्थनाएँ और निजी शोक मनाते हैं, लेकिन इन मौतों में योगदान देने वाले प्रणालीगत मुद्दों पर शायद ही कभी ध्यान देते हैं।
पादरियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य संसाधन सीमित हैं या मौजूद ही नहीं हैं। बिशप अक्सर ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ कमज़ोरियों को हतोत्साहित किया जाता है और पूर्णतावाद की प्रशंसा की जाती है।
धार्मिक भ्रम गहरा है। सुसमाचार कभी भी यीशु को भावनात्मक रूप से अजेय नहीं दिखाता। वह गतसमनी में रोया, अंधकार में सांत्वना ढूँढ़ी, और खुले तौर पर पीड़ा व्यक्त की। प्रारंभिक चर्च सफल रहा क्योंकि उसके नेता सच्चे इंसान थे, घायलों के मरहम लगाने वाले जो पीड़ा और आशा दोनों को समझते थे।
वियान्ने स्वयं इस बात को स्पष्ट करते हैं। उनका आत्म-संदेह, रातों की नींद हराम करना और कठोर आत्म-उपचार शुद्ध पवित्रता नहीं थे - उन्होंने प्रकट किया कि जब कोई व्यक्ति अकेले असहनीय बोझ उठाता है तो क्या होता है। उनके संघर्षों से हमें मानवीय सहयोग का महत्वपूर्ण महत्व सीखना चाहिए, न कि अलगाव का आधार प्रदान करना चाहिए।
चर्च को पुरोहित जीवन के बारे में अपने दृष्टिकोण पर मौलिक रूप से पुनर्विचार करना चाहिए। पुरोहित होने का अर्थ मौन पीड़ा की यात्रा नहीं है। यह एक आह्वान है जो ईश्वर और लोगों के साथ एकता में निहित है। एकता के लिए ईमानदारी, कमज़ोरी और आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। इसमें यह स्वीकार करना शामिल है कि पुरोहित भी इंसान हैं और उनकी भी बाकी सभी की तरह मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें हैं।
वास्तविक सुधार के लिए व्यावहारिक समायोजन की आवश्यकता होती है। धर्मप्रांतों को पादरियों के लिए व्यापक मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने चाहिए। सेमिनारियों को आध्यात्मिक विकास के साथ-साथ गंभीर मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण भी शामिल करना चाहिए।
बिशपों को ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जहाँ पादरियों को न्याय या करियर पर पड़ने वाले प्रभावों के डर के बिना मदद माँगने में सुरक्षित महसूस हो। पुरोहित बिरादरी को केवल औपचारिक समारोहों से आगे बढ़कर सच्ची मित्रता और सहयोग का एक माध्यम बनना चाहिए।